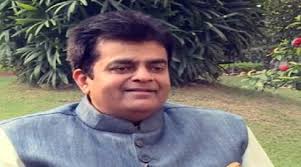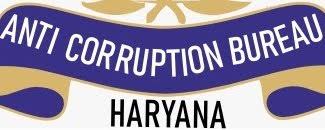अर्जुन सिंह
आज धीरे-धीरे हमारे सामाजिक और शैक्षिक विमर्श से ओझल होते जा रहे हैं।
इतिहास उन लोगों को हमेशा याद रखता है जिन्होंने अपने कर्मों से देश और समाज को दिशा दी। परंतु यह भी एक कटु सत्य है कि समय के साथ कुछ महान व्यक्तित्वों को हम भूलते जा रहे हैं। महाराणा प्रताप, जिनका नाम साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का पर्याय है, आज धीरे-धीरे हमारे सामाजिक और शैक्षिक विमर्श से ओझल होते जा रहे हैं। यह न केवल चिंताजनक है, बल्कि हमारे ऐतिहासिक बोध के लिए भी एक गंभीर संकेत है।
भारतीय इतिहास में एक ऐसे स्वाभिमानी योद्धा की कहानी जरूर कहता है
महाराणा प्रताप का जीवन केवल युद्धों और संघर्षों की गाथा नहीं है, बल्कि वह आत्मबल, स्वतंत्रता और आत्मगौरव का प्रतीक है। 1540 में मेवाड़ के राजा उदय सिंह के पुत्र के रूप में जन्मे महाराणा प्रताप ने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बजाय जीवन भर संघर्ष को चुना। उनका संपूर्ण जीवन इस बात की मिसाल है कि व्यक्ति सीमित संसाधनों के बावजूद अगर आत्मबल से भरा हो, तो वह किसी भी साम्राज्य के सामने टिक सकता है।
हल्दीघाटी का युद्ध चाहे रणनीतिक रूप से निर्णायक न रहा हो, लेकिन वह भारतीय इतिहास में एक ऐसे स्वाभिमानी योद्धा की कहानी जरूर कहता है जिसने गुलामी की जंजीरों को स्वीकार करने से बेहतर जंगलों में रहना उचित समझा। राणा प्रताप ने अपने परिवार और साथियों के साथ वर्षों तक जंगलों में कठिन जीवन बिताया, लेकिन अपनी स्वतंत्रता को कभी नीलाम नहीं किया। उनके घोड़े चेतक की वीरगाथा भी आज भी बच्चों को सुनाई जाती है, लेकिन केवल कहानी के रूप में, न कि प्रेरणा के रूप में।
युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कल्चर से जुड़ी हुई है
विडंबना यह है कि ऐसे नायक की स्मृति आज आधुनिक भारत में धूमिल होती जा रही है। विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताबों में महाराणा प्रताप को पर्याप्त स्थान नहीं दिया जाता। कई बार विदेशी शासकों को विस्तृत अध्यायों में पढ़ाया जाता है, जबकि अपने देश के योद्धाओं का उल्लेख कुछ पंक्तियों तक सीमित रह जाता है। क्या यह हमारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण की विफलता नहीं है?
आज की युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कल्चर से जुड़ी हुई है, लेकिन उसे यह समझाना आवश्यक है कि उसका मूल किस मिट्टी में है। महाराणा प्रताप केवल इतिहास के पन्नों का विषय नहीं हैं, वे एक जीवंत प्रेरणा हैं जो हमें यह सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी आत्मसम्मान और देशभक्ति से समझौता नहीं किया जा सकता।
उनकी जयंती को केवल रस्म अदायगी तक सीमित न रखते हुए एक प्रेरणादायक पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए।
मीडिया, खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इतिहास से जुड़े कंटेंट का प्रचलन बढ़ रहा है, लेकिन इसमें भी महाराणा प्रताप की झलक कम ही दिखाई देती है। टीवी सीरियल, फिल्में और वेब सीरीज अगर ऐतिहासिक विषयों पर बनती भी हैं, तो या तो वे अत्यधिक नाटकीय होती हैं या शोध की कमी से विकृत इतिहास प्रस्तुत करती हैं। एक सच्चे और संतुलित दृष्टिकोण से महाराणा प्रताप का जीवन आम जन तक पहुंचाना आवश्यक है।
सरकार और समाज दोनों को मिलकर यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे युवाओं को महाराणा प्रताप जैसे चरित्रों से जोड़ा जाए। विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम, निबंध प्रतियोगिताएं, और स्थानीय इतिहास की पढ़ाई जैसे उपाय इस दिशा में उपयोगी हो सकते हैं। साथ ही, उनकी जयंती को केवल रस्म अदायगी तक सीमित न रखते हुए एक प्रेरणादायक पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए।
महाराणा प्रताप को याद रखना केवल एक परंपरा का निर्वाह नहीं, बल्कि आत्मगौरव का उत्सव है।
आज जब दुनिया भर में लोग अपनी जड़ों की ओर लौटने की बात कर रहे हैं, तब हमें अपने इतिहास को फिर से समझने और अपनाने की जरूरत है। महाराणा प्रताप का जीवन हमें यह सिखाता है कि व्यक्तिगत लाभ से ऊपर राष्ट्र का स्वाभिमान होता है। उनका त्याग, धैर्य और संकल्प आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस दौर में था।
यदि हम अपने इतिहास को केवल अतीत की घटनाओं के रूप में देखते रहेंगे, तो हम न केवल अपनी विरासत से कटते जाएँगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी उस प्रेरणा से वंचित कर देंगे जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता है।
अंत में यही कहना चाहूँगा कि महाराणा प्रताप को याद रखना केवल एक परंपरा का निर्वाह नहीं, बल्कि आत्मगौरव का उत्सव है। हमें उन्हें नायक की तरह नहीं, मार्गदर्शक की तरह याद रखना होगा। तभी हम कह पाएँगे कि हमने अपने इतिहास, अपने गौरव और अपने सच्चे स्वाभिमान की रक्षा की है।
जब खबरें व्यापार बन जाएं: विश्वास कहां से लाएं?
लोकतंत्र की आधारशिला जिन स्तंभों पर टिकी होती है, उनमें मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में विशेष स्थान प्राप्त है। इसकी भूमिका किसी भी लोकतांत्रिक समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह जनता और सत्ता के बीच संवाद का माध्यम बनता है। मीडिया का मूल उद्देश्य होता है तथ्य प्रस्तुत करना, प्रश्न उठाना, समाज को सूचित और जागरूक बनाना। लेकिन वर्तमान समय में यह प्रश्न बार-बार उठ रहा है कि क्या मीडिया वास्तव में जनमत बना रहा है या उसे भ्रमित कर रहा है?
पहले के समय में मीडिया को निष्पक्ष, निर्भीक और सत्य का पक्षधर माना जाता था। अखबार, रेडियो और दूरदर्शन जैसे माध्यमों के माध्यम से जनता तक सूचनाएँ पहुँचाई जाती थीं और जनता का भरोसा मीडिया पर अडिग होता था। लेकिन अब मीडिया की दुनिया व्यापक रूप से बदल चुकी है। संचार के आधुनिक साधनों की तीव्रता, समाचार चैनलों की बाढ़, सामाजिक मीडिया की निरंतरता और विज्ञापन आधारित व्यावसायिक मॉडल ने मीडिया की दिशा और धार दोनों को बदल दिया है।
आज के समय में अनेक समाचार माध्यमों पर यह आरोप लगते हैं कि वे केवल टीआरपी या पाठक संख्या के पीछे भागते हैं। सत्यता, वस्तुनिष्ठता और संतुलन की जगह अब पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग, सनसनीखेज शीर्षक, और उथले विश्लेषणों ने ले ली है। बहस के नाम पर चलने वाले कार्यक्रमों में तथ्यों से अधिक वाचालता और पूर्वनिर्धारित विचारधाराएँ हावी दिखाई देती हैं।
झूठी खबरें (फर्जी समाचार), भ्रामक चित्र और अधूरी जानकारी समाज को गहरे भ्रम में डाल देती हैं।
इसके अतिरिक्त, सामाजिक मीडिया ने समाचार और सूचना के क्षेत्र में एक प्रकार की अराजकता उत्पन्न कर दी है। अब हर व्यक्ति सूचना का स्रोत बन गया है, लेकिन यह सूचना सत्य है या नहीं, इसकी पुष्टि करना कठिन हो गया है। झूठी खबरें (फर्जी समाचार), भ्रामक चित्र और अधूरी जानकारी समाज को गहरे भ्रम में डाल देती हैं। यह स्थिति तब और खतरनाक हो जाती है जब इनका उपयोग लोगों की भावनाओं को भड़काने, धार्मिक या जातिगत तनाव फैलाने, या चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है।
मीडिया का यह बदलता स्वरूप न केवल जनता को भ्रमित करता है, बल्कि लोकतंत्र की नींव को भी हिला सकता है। जब जनमत किसी पूर्व निर्धारित एजेंडे, अफवाह या असत्य सूचना के आधार पर बनता है, तो उसका प्रभाव देश के नीति-निर्माण, सामाजिक सौहार्द और न्याय व्यवस्था पर भी पड़ता है।
मीडिया की गिरती विश्वसनीयता का एक कारण यह भी है कि आज वह व्यावसायिक दबावों में घिर गया है। विज्ञापन से होने वाली आय, राजनीतिक समर्थन और दर्शकों की संख्या पर टिके मीडिया मॉडल ने उसे वस्तुनिष्ठता से दूर कर दिया है। अब समाचार भी एक ‘उत्पाद’ बन गया है जिसे बेचने के लिए साजिश, सनसनी और विरोध की चाशनी में लपेटा जाता है।
यह सोचना होगा कि क्या वे अपने अस्तित्व का उद्देश्य पूरा कर पा रहे हैं?
ऐसे में मीडिया को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। उसे यह याद रखना होगा कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति जनता का विश्वास है, और यदि यह विश्वास एक बार डगमगाया तो उसे पुन: प्राप्त करना अत्यंत कठिन होगा। मीडिया को चाहिए कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, रोजगार, महिला सुरक्षा जैसे वास्तविक मुद्दों को प्राथमिकता दे। साथ ही, उसे सत्य, संतुलन और विवेक से युक्त रिपोर्टिंग करनी चाहिए, न कि भेदभावपूर्ण और उत्तेजनात्मक सामग्री प्रसारित करनी चाहिए।
मीडिया संस्थानों के लिए यह समय आत्मसमीक्षा का है। उन्हें यह सोचना होगा कि क्या वे अपने अस्तित्व का उद्देश्य पूरा कर पा रहे हैं? क्या वे समाज में जागरूकता फैला रहे हैं या भ्रम पैदा कर रहे हैं? क्या वे जनता के मुद्दे उठा रहे हैं या सत्ताधारियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं?
समाज और लोकतंत्र के हित में यही आवश्यक है कि मीडिया फिर से अपनी वास्तविक भूमिका को पहचाने। वह न तो केवल मनोरंजन का साधन बने, न ही किसी विचारधारा का प्रवक्ता। उसे लोकतंत्र की आत्मा के रूप में सत्य और विवेक का प्रतिनिधित्व करना होगा।